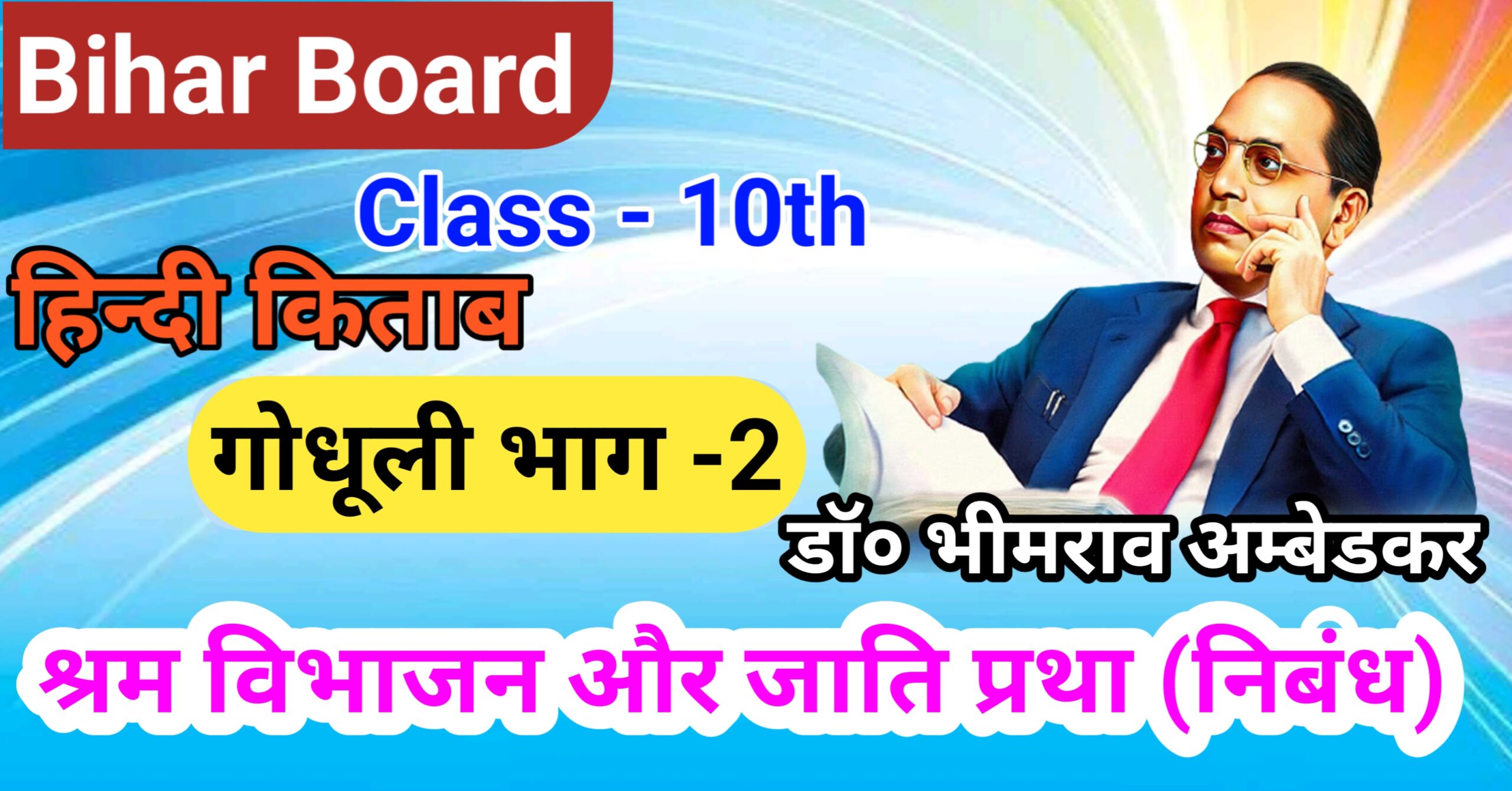जय हिन्द। इस पोस्ट में बिहार बोर्ड क्लास 10 हिन्दी किताब गोधूली भाग – 2 के गद्य खण्ड के पाठ एक ‘श्रम विभाजन और जाति प्रथा’ के सारांश को पढ़ेंगे। इस निबंध के लेखक भीमराव अम्बेडकर है । अम्बेडकर जी ने इस निबंध के माध्यम से लोगों में मानवीयता, सामाजिक सद्भावना, समरसता जैसे मानवीय गुणों का विकास करने का प्रयत्न किया गया है।|(Bihar Board Class 10 Hindi भीमराव अम्बेडकर) (Bihar Board Class 10 Hindi श्रम विभाजन )(Bihar Board Class 10th Hindi Solution) ( श्रम विभाजन और जाति प्रथा ) (Shram Vibhajan Aur Jati Pratha Question Answer)
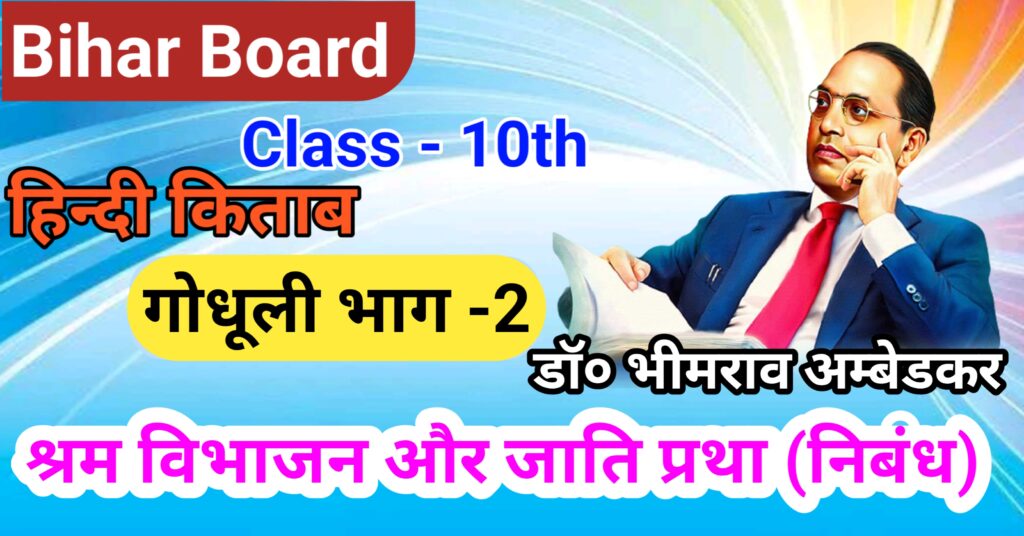
श्रम विभाजन और जाति प्रथा
श्रम विभाजन और जाति प्रथा : लेखक परिचय
- लेखक का नाम – डॉ० भीमराव अम्बेडकर
- जन्म – 14 अप्रैल 1891 ई०
- जन्म स्थान – महु, मध्य प्रदेश
- मृत्यु – 6 दिसंबर 1956 ई० ( दिल्ली में )
- पिता का नाम – रामजी सकपाल
- माता का नाम – भीमा बाई०
- प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क ( अमेरिका ) तथा लंदन ( इंग्लैंड ) गए।
- इन्होंने PhD की उपाधि 1916 में धारण की।
- कुछ दिनों तक वकालत करने बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए।
- इनके तीन प्रेरण – बुद्ध , कबीर और ज्योतिबा फूले
- प्रमुख रचनाएँ — ‘द कास्ट्स इन इंडिया : देयर मैकेनिज्म’, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट’, ‘द अनटचेबल्स, हू आर दे’, ‘हू आर शूद्राज’, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म’, बुद्धा एण्ड हिज धम्मा’, ‘थाट्स ऑन लिंग्युस्टिक स्टेट्स’, ‘द राइज एंड फॉल ऑफ द हिन्दू वीमेन’, ‘एनीहिलेशन ऑफ कास्ट’ आदि ।
- पत्रिका – मुकनायक
- भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से ‘बाबा साहब अंबेदकर संपूर्ण वाङ्मय’ नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है।
- इनको संविधान के निर्माता कहकर संबोधित करके श्रद्धांजलि अर्पित करते है।
- यह पाठ एनीहिलेशन ऑफ कास्ट’ ( भाषण ) से ली गई है।
- यह भाषण ‘जाती – प्रथा तोड़क मंडल’ ( लाहौर ) के वार्षिक सम्मेलन ( सन् 1936 ) में हुआ था।
- इसका हिन्दी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया है।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा : पाठ परिचय
प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेत्ता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है ।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा
पाठ का सारांश
प्रस्तुत पाठ ‘श्रम विभाजन और जाति प्रथा’ में लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमानता के विरूद्ध अपना विचार प्रकट किया है।
लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में भी कुछ लोग ‘जातिवाद’ के कटु समर्थक हैं, उनके अनुसार कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है। परन्तु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक-दूसरे की अपेक्षा ऊँच-नीच भी करार देती है।
जाति-प्रथा को यदि श्रम-विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रूचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्त्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपने रूचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। इस सिद्धांत के विपरित जाति-प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता-पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबुर होना पड़ता है।
जाति-प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बाँध भी देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। इसलिए भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है।
जाति-प्रथा से किया गया श्रम-विभाजन किसी की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। जिसके कारण लोग निर्धारित कार्य को अरूचि के साथ विवशतावश करते हैं। इस प्रकार जाति-प्रथा व्यक्ति की स्वभाविक प्रेरणारुचि व आत्म-शक्ति को दबाकर उन्हें स्वभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है।
समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि आर्दश समाज वह है, जिसमें स्वतंत्रता, समता, भातृत्व को महत्व दिया जा रहा हो। दूध पानी के मिश्रण की तरण भाईचारे का वास्तविक रूप हो।
श्रम विभाजन और जाति प्रथा : पाठ्य पुस्तक के प्रश्न (Shram Vibhajan Aur Jati Pratha Question Answer)
प्रश्न 1. लेखक किस विडंबना की बात करते हैं ? विडंबना का स्वरूप क्या है ?
उत्तर –लेखक भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के पोषकों को विडंबना की बात कह कर संबोधित किया है। विडंबना का स्वरूप यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिक विभाजन का भी रुप है। यह जाति प्रथा मजदूरों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊँच – नीच भी करार देती है।
(Shram Vibhajan Aur Jati Pratha Question Answer)
प्रश्न 2. जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं ?
उत्तर – जातिवादियों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। यह श्रम विभाजन जाति प्रथा का ही दूसरा रूप है। हिन्दू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। परंपरागत पेशे में व्यक्ति निपुण हो जाता है और अपना कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता है।
प्रश्न 3. जातिवाद के पक्ष में दिए गए तकों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या हैं ?
उत्तर –जातिवाद के पक्ष में जो भी तर्क दिए गए हैं उन सभी तर्कों पर लेखक ने आपत्तियाँ प्रकट करते हुए कहा है कि जाति प्रथा गंभीर दोषों से परिपूर्ण है। यह श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत रूचि का इसमें कोई महत्व नहीं है। यह आर्थिक पहलू से भी ज्यादा हानिकारक है। वास्तव में यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि तथा आत्म शक्ति को दबा देती है और उसे निष्क्रिय बना देती है।
प्रश्न 4. जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती ?
उत्तर – इसका वास्तविक कारण यह है कि, यह व्यक्ति की रुचि और योग्यता का ध्यान नहीं रखती बल्कि मनुष्य को उसके परंपरागत पेशे में उलझा कर , जिन्हें मानने के लिए मजबूर कर देती है।
(Shram Vibhajan Aur Jati Pratha Question Answer)
प्रश्न 5. जातिप्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है ?
उत्तर –हिन्दू धर्म में जो जाति प्रथा है वह किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। भले ही वह उसमें पारंगत ना हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है।
प्रश्न 6 लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों ?
उत्तर –डॉ० भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रूचि का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है।
प्रश्न 7. लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है ?
उत्तर –जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन हो गया है। आपस में ऊंच-नीच की भावना भी उपस्थित है। जाति प्रथा के कारण ही बिना इच्छा के पैतृक पेशा को अपनाना पड़ता है जिसके कारण मनुष्य की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं होता है। आर्थिक विकास में भी जाति प्रथा बाधा उत्पन्न करती है।
प्रश्न 8. सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है ?
उत्तर – सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित आदर्श समाज चाहता है। आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए ताकि कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप हो। इसी का नाम लोकतंत्र है। अनुभवों का आदान-प्रदान ही लोकतंत्र है।
Shram Vibhajan Aur Jati Pratha Question Answer
बिहार बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें!यहाँ आपकोClass 6th से 12thतक सभी विषयों के Solutions, Notes और महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्यामिलेंगी। अभी सब्सक्राइब करें और टॉप करें!
🔴देखें –Click Here